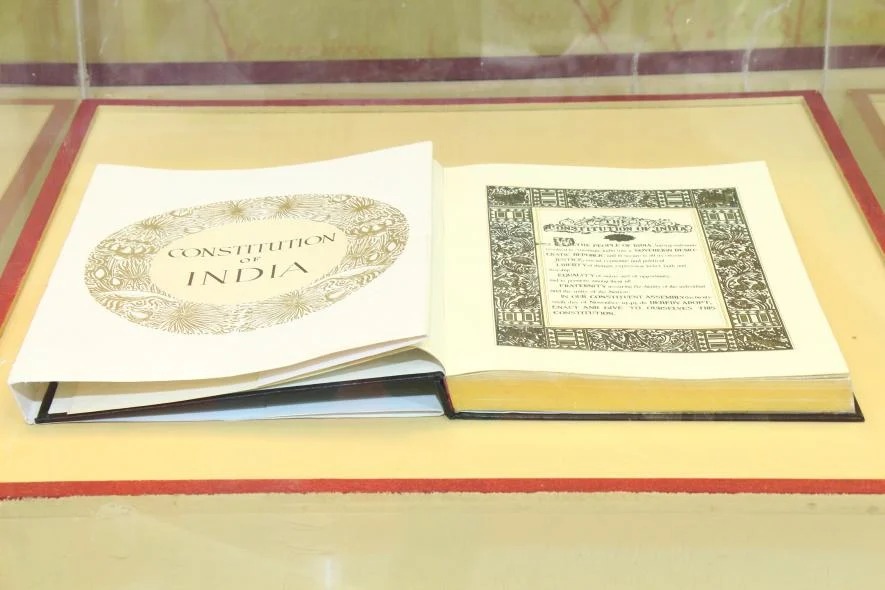19 दिसंबर क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफ़ाक़उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह की शहादत का दिन है. आज जब देश की आज़ादी और लोकतंत्र गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ज़रूरी हैं कि देशवासी शहीदों की स्मृतियां खंगालकर उनके व्यक्तित्व से नई प्रेरणा, नया बल प्राप्त करें.
मरते बिस्मिल, रोशन, लहरी, अशफाक अत्याचार से / पैदा होंगे सैकड़ों उनके रुधिर की धार से/ उनके प्रबल उद्योग से उद्धार होगा देश का/ तब नाश होगा सर्वथा दुख शोक के लवलेश का.
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचआरए) से संबद्ध उद्भट क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने ये पंक्तियां उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जेल में 1927 में आज ही के दिन हुई अपनी शहादत से महज कुछ दिनों पहले रची थीं.
अब यह तो सुविदित ही है कि बीती शताब्दी के तीसरे दशक में धन की कमी इस एसोसिएशन द्वारा स्वतंत्रता के लिए संचालित सशस्त्र क्रांतिकारी संघर्ष के आड़े आने लगी तो उसने तय किया कि उसके क्रांतिकारी अत्याचारी गोरी सरकार का वह खजाना (उसके मतानुसार जिसे उसने देश की जनता की चौतरफा व खुल्लमखुल्ला लूट से इकट्ठा कर रखा था) बलपूर्वक लूट लेंगे और उससे ही लड़ने में इस्तेमाल करेंगे. इसी निश्चय के तहत उन्होंने नौ अगस्त, 1925 को आठ डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में ले जाया जा रहा सरकारी खजाना काकोरी स्टेशन के पास लूट लिया था. इस लूट को इतिहास अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानता है और यह इसका शताब्दी वर्ष है.
तब देश की गोरी सरकार इस एक्शन से अंदर तक हिल गई थी और उसने मुकदमे का नाटक कर इसके चार नायकों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्लाह खां, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, गोंडा और मलाका (इलाहाबाद) जेलों में फांसी पर लटकाकर शहीद कर डाला था.
इन चारों की फांसी के लिए उन्नीस दिसंबर, 1927 की तारीख तय थी, लेकिन मदांध सरकार ने इस अंदेशे से आतंकित होकर लाहिड़ी को दो दिन पहले 17 दिसंबर को ही शहीद कर डाला था कि एचआरए ने उन्हें छुड़ाने की योजना बना ली है और उसके क्रांतिकारी कभी भी गोंडा जेल पर हमला करके उनको छुड़ा ले जाएंगे.
आज, जब काकोरी एक्शन के शताब्दी वर्ष में भी देश की आज़ादी और लोकतंत्र गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उसकी यादें इस अर्थ में बहुत जरूरी हैं कि देशवासी (जिनमें से अनेक अब इस हद तक निराश हो चले हैं कि उन्हें इस रात की कोई सुबह या तो दिखाई ही नहीं देती या बहुत दूर दिखाई देती है) उसके शहीदों की स्मृतियां खंगालकर उनके व्यक्तित्व व कृतित्व से नई प्रेरणा व नया बल प्राप्त कर सकते हैं.
हां, यह संदेश भी कि स्वतंत्रता के लिए या उसकी चुनौतियों से पार पाने के लिए किए जाने वाले संघर्ष न कभी स्थगित होते हैं और न उनमें निराशा के लिए कोई जगह होती है. बिस्मिल की उक्त पंक्तियां साक्षी हैं कि क्रांतिकारियों ने अपने संघर्ष में शहादतों के वक्त भी निराशा के लिए कोई जगह नहीं रखी थी.
इसके उलट वे सब के सब इस विश्वास से भरे हुए थे कि उनकी शहादत के बाद आने वाली देश की नई युवा पीढ़ियां उनके अरमानों को मंजिल तक पहुंचा देंगी.
‘ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश चाहता हूं’
उल्लेखनीय है कि यह विश्वास इस तथ्य के बावजूद था कि उनका सामना ऐसे महाशक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से था, जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था. गौरतलब है कि इन क्रांतिकारियों के चार साल बाद 23 मार्च,1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने शहादत पाई, तो भी उनका जीत का जज्बा कमजोर नहीं ही पड़ा था.
शहीद-ए-आजम भगत सिंह को तो लगता था कि उनकी शहादत से देश के युवाओं में देशप्रेम का अभूतपूर्व जज्बा पैदा हो जाएगा और आज़ादी के लिए बलिदान देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अभीष्ट क्रांति को रोक पाना ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बूते की बात नहीं रह जाएगी. इसीलिए उन्होंने अपनी शहादत के बाद भी हर तरह के ज़ुल्म, शोषण व गैरबराबरी के खात्मे तक ‘युद्ध’ जारी रहने का ऐलान किया था.
इतना ही नहीं, सात अक्तूबर, 1930 को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद देश में कई स्तरों पर उन्हें बचाने के प्रयत्न आरंभ हुए, तो वे उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहकर मांग करते रहे थे कि उन्हें फांसी देने के बजाय युद्धबंदी मानकर गोली से उड़ा दिया जाए. क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है और इस बात को वे छुपाते भी नहीं हैं.
बहरहाल, अपने 30 वर्ष के जीवन में 11 वर्ष स्वतंत्रता संघर्ष को समर्पित कर देने वाले बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में (जिसका अंतिम अध्याय उन्होंने अपनी शहादत से तीन दिन पहले ही पूरा किया था) लिखा है कि ‘न मैं प्राण त्यागते समय निराश हूं और न यह सोचता हूं कि हम लोगों के बलिदान व्यर्थ गए.’
उनको लगता था कि ‘हम लोगों की छिपी हुई आहों का असर सामने आने लगा है और गुलामी की जंजीरें अंततः टूटकर ही रहेंगी.’ इसीलिए उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने बेलाग-लपेट कह दिया था : आई विश द डाउनफॉल आफ ब्रिटिश एंपायर (यानी मैं ब्रिटिश साम्राज्य का नाश चाहता हूं.)
उनके साथी राजेंद्रनाथ लाहिड़ी तो इसे लेकर भी गौरवान्वित थे कि उन्हें अपने साथियों से दो दिन पहले शहादत देने का मौका मिला. वे इतने जोश में थे कि अपनी शहादत के दिन भी उन्होंने व्यायाम किया और इससे चकित जेलर के पूछने पर उसका उद्देश्य बताया था कि वे अगले जन्म में भी ऐसे ही गठीले और स्वस्थ शरीर के साथ पैदा होना चाहते हैं. ताकि स्वतंत्रता का जो संघर्ष इस जन्म में अधूरा रह गया है, उसे पूरा करने में नई भूमिका निभा सकें.
दूसरी ओर मलाका जेल में रोशन सिंह को जिंदादिली के बगैर जिंदगी ही बेकार लगती थी. आखिरी वक्त में उन्होंने कहा था: जिंदगी जिंदादिली को मान ऐ रोशन/ वरना कितने ही यहां रोज फना होते हैं.
गैरबराबरी कतई कुबूल न थी
अशफाक की बात करें, तो जालिमों के जुल्म से तंग आकर जिंंदान-ए-फैजाबाद से बेदाद से सू-ए-अदम चल देने से पहले उनकी अंतिम इच्छा थी कि जब उन्हें फांसी पर लटकाया जाए तो उनके वकील फांसी घर के सामने खड़े होकर देखें कि वे कितनी खुशी और हसरत से उसके फंदे पर झूल रहे हैं.
अशफाक को विदेशी तो क्या ऐसी स्वदेशी जम्हूरी सल्तनत भी कुबूल नहीं थी, जिसमें कमजोरों का हक, हक न समझा जाए, जो हुकूमत के सरमायादारों व जमीनदारों के दिमागों का नतीजा हो, जिसमें मजदूरों व काश्तकारों का बराबर हिस्सा न हो या जिसमें ‘बाहम इम्तियाज व तफरीक रखकर हुकूमत के कवानीन (कानून) बनाये जाएं’.
अरसे तक गुमनामी में कोई रही अपनी जेल डायरी में वे लिख गए हैं कि अगर आज़ादी का मतलब इतना ही है कि गोरे आकाओं के बजाय हमारे वतनी भाई सल्तनत की हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में ले लें और अमीर व गरीब, जमीनदार व काश्तकार में तफरीक (गैरबराबरी) कायम रहे तो ऐ खुदा मुझे ऐसी आज़ादी उस वक्त तक न देना, जब तक तेरी मखलूक में मसावात (यानी बराबरी) कायम न हो जाए.
अपनी डायरी में आगे उन्होंने यह भी लिखा है कि ऐसे खयालों के लिए उनको इश्तिराकी (यानी कम्युनिस्ट) समझा जाए तो भी उन्हें इसकी फिक्र नहीं. अपनी शहादत से पहले एक संदेश में उन्होंने उन दिनों देश में सक्रिय कम्युनिस्ट ग्रुप से गुजारिश की थी कि वह जेंटलमैनी छोड़कर ऐसी आज़ादी के लिए काम करे, जिसमें गरीब खुश और आराम से रहें और सब बराबर हों.
उन्होंने कामना की थी कि उनकी शहादत के बाद वह दिन जल्द आए, जब छतर मंजिल लखनऊ में अब्दुल्ला मिस़्त्री व धनिया चमार, किसान भी, मिस्टर खलीकुज्जमा और जगतनारायण मुल्ला व राजा महमूदाबाद के सामने कुर्सी पर बैठे नजर आएं, जबकि अपने लिए उनकी आरजू महज इतनी-सी थी कि ‘रख दे कोई जरा सी खाकेवतन कफन में’.
सर वाल्टर स्काॅट की नज्म ‘लव आफ कंट्री’ के साथ स्पार्टा के वीर होरेशस के किस्से को वे अपने क्रांतिकारी जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बता गए हैं. उन्होंने लिखा है कि जब वे आठवां दर्जा पास होकर आए और उनके अध्यापक ने अपने देश को बचाने के लिए होरेशस के टाइबर नदी पर बना पुल तोड़कर दुश्मन सेनाओं को आने से रोकने और तब तक संकरे रास्ते पर तीन साथियों के साथ खड़े होकर लड़ने का वाकया सुनाया तो वे खासे भावावेश में आ गए थे.
उन्होंने अपने वतन से मुहब्बत की अदाओं को बेहद निराली और अनोखी बताते हुए लिखा है कि वरना यह आसान काम नहीं कि कोई इंसान मौत का मुकाबला करने के लिए अपने को इतनी खुशी से पेश करे.
उठो-उठो सो रहे हो नाहक
साफ है कि आज़ादी के लिए दी गई शहादतें देश की ऐसी शक्ल-व-सूरत के लिए कतई नहीं थीं, जैसी इन दिनों बना (पढ़िए: बिगाड़) डाली गई हैं. यकीनन, उसकी इस बदशक्ली का एक बड़ा कारण यह है कि वह नामुकम्मल काम अभी भी पूरा होना बाकी है, अशफाक और उनके साथी जिसके लिए मैदान-ए-अमल तभी तैयार कर गए थे और युवाओं से कहा था-‘उठो-उठो सो रहे हो नाहक!’
उस काम के अधूरे होने के ही कारण आज देश की कई पीढ़ियां एक साथ व्यथित और विचलित दिखाई देती हैं. सबसे ज्यादा वह पीढ़ी, जिसने न सिर्फ अपने समय में गुमी हुई आज़ादी की कीमत पहचानी बल्कि उसे ढूंढ लाने के लिए एड़ी-चोटी का पसीना एक किया और जो खत्म होती-होती विलुप्ति के कगार पर जा पहुंची है. लेकिन वे पीढ़ियां भी कुछ कम विचलित नहीं, जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुईं और नाना प्रकार की पतनशील प्रवृत्तियों के बीच पली-बढ़ी हैं. भले ही अलग-अलग कारणों से, मगर एक जैसी तकलीफों से दो-चार होने के कारण, कई बार ये सारी एक जैसी कातर होकर आर्त हो उठती हैं.
इन शहीदों की ओर देखकर उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है: निराशा से कभी भी कुछ भी हासिल नहीं होता. जुल्मतों के इन काले दिनों में भी नहीं ही हासिल होगा. जो भी हासिल होगा, यह समझकर हालात बदलने के प्रयत्न करने से होगा कि घटायें कितनी भी काली क्यों न हों, वे सूरज को बहुत देर तक ढके नहीं रख पातीं. हमारे शहीदों ने उस गुलामी के घुप्प अंधेरे में भी हिम्मत नहीं हारी थी तो हम इस नई गुलामी की माया को ही अजेय मानकर निराश क्यों हों भला?
Source: The Wire