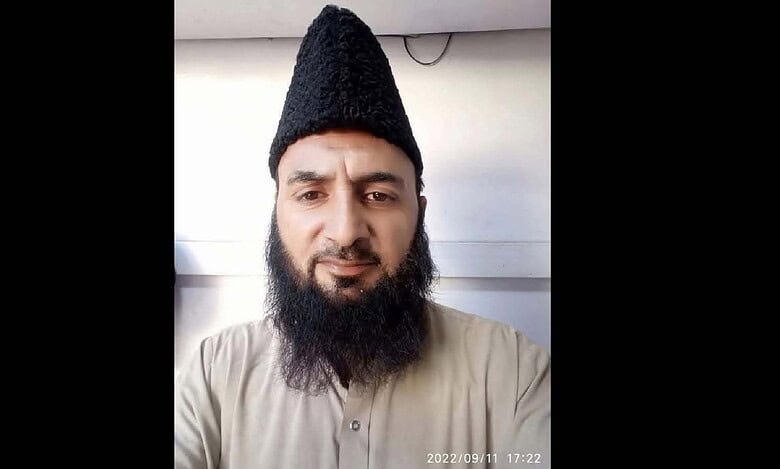ट्रंप द्वारा छेड़ा गया व्यापार युद्ध कई आयामों वाला है। यह सिर्फ़ चीन, यूरोपीय संघ, जापान और भारत जैसे बड़े देशों के खिलाफ़ नहीं, बल्कि लेसोथो जैसे छोटे और ग़रीब देशों को भी निशाना बनाता है—लेसोथो, जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में है, अमेरिका को हीरे निर्यात करता है और जिसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग $3.3 है। उसकी अमेरिका से कोई ख़रीदने की औकात नहीं है, फिर भी अमेरिका ने उस पर 50% आयात शुल्क थोप दिया—किसी भी देश पर लगाया गया अब तक का सबसे ऊँचा टैरिफ़।
ट्रंप की यह विचित्र टैरिफ़ नीति अंटार्कटिका के उन द्वीपों तक जा पहुँची, जहाँ केवल पेंगुइन रहते हैं, और डिएगो गार्सिया जैसे सैन्य अड्डों तक भी, जहाँ केवल अमेरिकी सैनिक रहते हैं। यह टैरिफ़ मैक्सिको और कनाडा जैसे देशों को भी नहीं बख्शते—भले ही वे अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements) में बँधे हों—या जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और फ़िलीपींस जैसे संधि-सहयोगियों को। भारत और वियतनाम जैसे देश तो “मित्रता के तीसरे घेरे” में आते हैं—अगर ट्रंप और अमेरिका के पास अब कोई मित्र बचे हों तो!
मैं यहाँ यह विश्लेषण नहीं करने जा रहा कि मुक्त व्यापार (Free Trade) का असली लाभ अमीर देशों को क्यों मिलता है, ट्रंप की टैरिफ़ नीति की आलोचना भले सही हो पर कारण ग़लत हैं, या फिर विकासशील देशों के लिए क्या नीति बेहतर होगी—एक प्रकार का आत्मनिर्भर मॉडल या फिर स्पष्ट लक्ष्य के साथ योजना बद्ध सहभागिता। आज का यथार्थ यह है कि वैश्विक पूंजी का संकट साफ़ दिखा रहा है कि “मुक्त” व्यापार और पूंजी प्रवाह की नीति अब अमीर देशों के लिए भी कारगर नहीं रह गई है। ट्रंप का मानना है कि अब एक नई रणनीति की ज़रूरत है—और वह रणनीति है आर्थिक तबाही का नया डिज़ाइन, जिसकी नींव उन्होंने टैरिफ़ युद्ध पर रखी है।
ट्रंप की टीम का व्यापार संतुलन का सिद्धांत भी अजीब है—वो किसी भी देश के अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष को उसके अमेरिका को किए गए निर्यात से विभाजित करते हैं। अगर यह अनुपात नकारात्मक है (यानी अमेरिका का उस देश के साथ अधिशेष है), तब भी उस देश पर न्यूनतम 10% का टैरिफ़ लगाया जाएगा। अगर अनुपात सकारात्मक है, तो उसके आधे हिस्से को टैरिफ़ बना दिया जाएगा—पर 10% की न्यूनतम सीमा लागू रहेगी। इस तरह, अमेरिका चाहता है कि वह हर देश से न सिर्फ़ व्यापार में मुनाफ़ा कमाए, बल्कि हर देश के साथ अपना हिसाब भी बराबर करे—भले ही वैश्विक व्यापार संतुलन का सिद्धांत यह हो कि किसी देश का किसी एक से घाटा हो सकता है, तो किसी दूसरे से लाभ भी।
यही हास्यास्पद “सिद्धांत” और उसकी गणनाएं अमेरिकी स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट को धराशायी कर गईं, और ट्रंप को कुछ कदम पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन टैरिफ़ की धमकी अभी भी पूरी दुनिया पर मंडरा रही है। चीन के साथ अमेरिका का व्यापार युद्ध जारी है और और भी ज़्यादा तीखा होता जा रहा है।
टैरिफ़ थोपने के फ़ौरन बाद अमेरिका के शेयर बाजार में गिरावट आई, जो बॉन्ड बाज़ार तक भी पहुँच गई। अमेरिकी ट्रेज़री बॉन्ड वाला बॉन्ड बाज़ार, शेयर बाज़ार से भी बड़ा है। इस बॉन्ड मार्केट के धराशायी होने के डर से ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। याद कीजिए, जब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज़ ट्रस ने 2022 में अपना विनाशकारी बजट पेश किया था और बॉन्ड मार्केट ध्वस्त हो गया था, तो उन्हें 49 दिनों में ही इस्तीफ़ा देना पड़ा था।
अब ट्रंप ने नए टैरिफ़ पर 90 दिनों की “छूट” की घोषणा की है—इस अवधि में सभी देशों को अमेरिका से आकर वार्ता करनी होगी। मगर 10% का न्यूनतम टैरिफ़ और कुछ अन्य शुल्क जारी रहेंगे। ये खुली चेतावनी है: अगर कोई देश अपने टैरिफ़ में छूट चाहता है, तो उसे ‘सम्राट ट्रंप’ के दरबार में आकर झुकना होगा। चाहे किसी देश का अमेरिका से व्यापार घाटा हो और वह अमेरिका पर कोई टैरिफ़ न लगाता हो, फिर भी उसे यह 10% शुल्क देना ही होगा—यह “अपरिहार्य” है।
फिच रेटिंग के मुताबिक, इन तथाकथित “छूटों” के बावजूद अमेरिका का औसत टैरिफ़ 2024 के 2.5% से उछलकर 22% तक पहुँच गया है—जो कि 1910 के बाद से सबसे ज़्यादा है।
अधिकतर देश अब अमेरिका से बातचीत करने लगे हैं। मगर चीन ने ट्रंप के साथ खेलने से इनकार कर दिया और बराबर की प्रतिक्रिया में अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ़ लगा दिए। इसके जवाब में अमेरिका ने चीन पर टैरिफ़ को 145%–175% तक बढ़ा दिया। चीन का टैरिफ़ 125% पर रोक दिया गया है, क्योंकि चीन का मानना है कि इस सीमा के बाद व्यापार लगभग असंभव हो जाता है और उस पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क केवल दिखावा भर है।
विश्व व्यापार संगठन (WTO) के साथ जो व्यापारिक व्यवस्था बनाई गई थी, वह इस धारणा पर आधारित थी कि अमीर देश—खासकर अमेरिका—विज्ञान और तकनीक में अपनी बढ़त से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखेंगे। यानी, गरीब देश निम्न-तकनीकी उत्पाद बनाएंगे और अमीर देश उच्च-तकनीकी उत्पादों से मुनाफ़ा कमाएँगे। जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, अमीर देश उससे भी ऊँची तकनीक की ओर बढ़ेंगे और बाकी सब पीछे छूट जाएंगे। यह कोई पूरी तरह उपनिवेशवादी मॉडल तो नहीं था, लेकिन उसका ही एक परिष्कृत रूप था।
फिर भी WTO ढाँचे में राज्य की भूमिका बनी रही—तकनीकी विकास में निवेश और उसे उद्योग से जोड़ने के लिए। भारत ने WTO में बौद्धिक संपदा (IP) के नियमों पर जो छूटें हासिल की थीं, उसी के बल पर हम ‘दुनिया की फार्मेसी’ बन सके। अफ़सोस की बात यह है कि अब यह स्थान भी हम चीन को सौंपते जा रहे हैं क्योंकि हम दवाओं के मूल घटक (Active Pharmaceutical Ingredients – APIs) के विकास की बजाय केवल अंतिम फॉर्मूलेशन पर ध्यान दे रहे हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भी हमने एकतरफा नीति अपनाई—सिर्फ़ सॉफ्टवेयर पर ध्यान दिया और हार्डवेयर को चीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान के हवाले छोड़ दिया। जबकि कभी C-DoT ने डिजिटल स्विच तकनीक में विकासशील देशों में अग्रणी भूमिका निभाई थी। दुर्भाग्य से हमारी योजना बनाने वाली “ब्राह्मणवादी” सोच—शायद हाथ से काम करने को हीन मानने के कारण—ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयुक्त विकास की कल्पना नहीं की।
दिलचस्प है कि अंतरराष्ट्रीय बिजनेस मीडिया, खासकर पश्चिमी प्रेस जैसे Financial Times, Bloomberg आदि, यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अमेरिका का यह व्यापार युद्ध अंततः उसी के लिए मुसीबत बन जाएगा। The Economist ने एक व्यंग्यपूर्ण शीर्षक भी दिया: “How America Could Make China Great Again”। दरअसल व्यापार युद्ध हर किसी को नुकसान पहुंचाता है—सवाल यह है कि किसे ज़्यादा नुकसान होता है? इस हानि-हानि के खेल में ट्रंप मानते हैं कि चीन ज़्यादा चोट खाएगा और पहले झुकेगा।
लेकिन जैसा कि Foreign Affairs पत्रिका में एडम पोसेन लिखते हैं, ट्रंप की यह सोच पूरी तरह ग़लत है। चीन चाहे तो घरेलू बाज़ार में मांग बढ़ाकर या अन्य देशों को निर्यात करके अपनी भरपाई कर सकता है। मगर अमेरिका के लिए चीन का विकल्प खोजना कहीं ज़्यादा मुश्किल है—खासकर उस पैमाने पर जिस पर उसे आपूर्ति चाहिए। चीन अमेरिका से सोयाबीन, तिलहन, ज्वार आदि कृषि उत्पाद खरीदता है—और यदि यह बंद हो गया तो ट्रंप के वोट बैंक को सीधी चोट लगेगी। Game theory में इसे escalation dominance कहा जाता है—यानी, उस पक्ष की जीत, जो दूसरे को अधिक दर्द दे सकता है। और इस व्यापार युद्ध में पोसेन के मुताबिक़, चीन के पास यह बढ़त है।
Apple और अन्य अमेरिकी कंपनियों पर पड़ने वाले असर को देख कर ट्रंप प्रशासन ने चीनी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर 145% टैरिफ़ में कुछ छूट दी—जिससे iPhone और लैपटॉप कंपनियों को थोड़ी राहत मिली। लेकिन जब तक यह युद्ध जारी रहेगा, ये कंपनियाँ हर समय तलवार की धार पर चलेंगी।
यह स्पष्ट है कि WTO की बनाई व्यापार व्यवस्था अब ख़त्म हो चुकी है—और वही देश जिन्होंने इसे खड़ा किया था, अब इसे दफ़न कर रहे हैं। चीन, दक्षिण कोरिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत के उभार ने पश्चिमी—या कहें पूर्व और नव-औपनिवेशिक देशों—को डरा दिया है। अब वे अपनी घटती ताक़त के बावजूद पूरी व्यवस्था को “मैं जीतूं तो ठीक, वरना तुम हारो” के उसूल पर ढालना चाहते हैं। वे यह युद्ध भले जीत न सकें, पर दुनिया की अर्थव्यवस्था को भारी नुक़सान पहुँचा सकते हैं—यही ट्रंप के टैरिफ़ युद्ध की ब्लैकमेलिंग है।
उनकी यह मानसिकता लुई XV के उस कथन जैसी है—“मेरे बाद तूफ़ान!” (Après moi, le déluge)—जिसका नतीजा फ्रांसीसी क्रांति के रूप में सामने आया था। ट्रंप अपने करियर में छह बार दिवालिया हो चुके हैं, लेकिन यदि यह वैश्विक आर्थिक दिवालियापन हुआ, तो यह केवल ट्रंप और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा—इसकी मार हम सब झेलेंगे।
Source: News Click