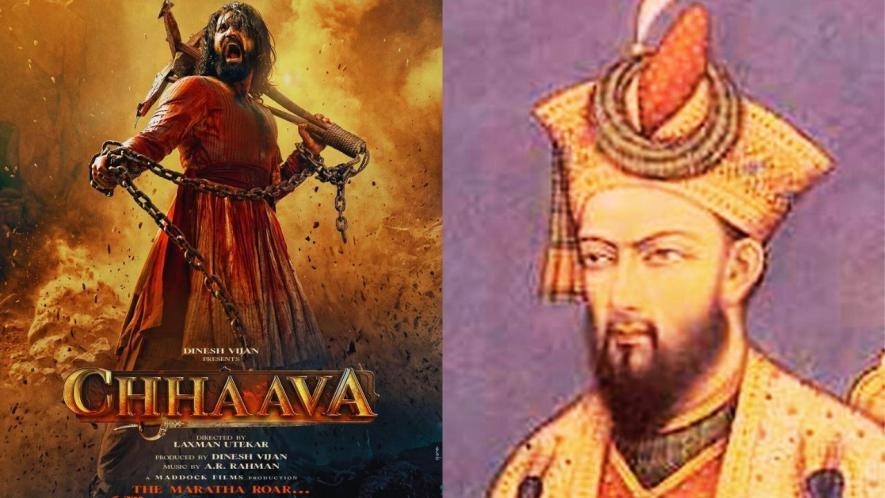एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स-स्टारलिंक का भारत की दो प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों—रिलायंस जियो और भारती एयरटेल—के साथ गठजोड़ कई सवाल खड़े करता है। मुख्य सवाल यह हैं:
- क्या इससे टेलीकॉम सेवाओं में एकाधिकार बढ़ेगा?
- क्या सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को बिना नीलामी के स्टारलिंक को दिया जाएगा?
इसके अलावा, यह सवाल भी उठता है कि क्या इस तरह से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति को व्यावसायिक उपयोग के लिए देना उचित है?
रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ गठजोड़ के बाद, स्टारलिंक को स्पेक्ट्रम आवंटन की प्राथमिकता मिलना तय लग रहा है। इससे भारत के टेलीकॉम बाज़ार में जियो और एयरटेल का दोध्रुवीय वर्चस्व और मजबूत होगा। अन्य कंपनियाँ, जैसे वोडाफोन आइडिया और सरकारी बीएसएनएल, इस दौड़ में पीछे रह जाएँगी।
क्या सरकार को इस तरह के बाज़ार संकेन्द्रण (consolidation) की अनुमति देनी चाहिए?
क्या इससे प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों की ताकत और एकाधिकार नहीं बढ़ेगा?
साथ ही, इन दोनों कंपनियों को महत्वपूर्ण संचार सेवाओं के लिए एक अमेरिकी कंपनी पर निर्भर होना पड़ेगा। क्या यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के खिलाफ नहीं है?
रणनीतिक संसाधनों पर विदेशी नियंत्रण का सवाल
बड़ा सवाल यह भी है कि एक स्वतंत्र भूमिका निभाने का दावा करने वाली सरकार क्या अपनी रणनीतिक टेलीकॉम संपत्तियों को किसी विदेशी कंपनी के नियंत्रण में जाने देगी?
यदि भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों और स्टारलिंक के बीच ऐसा गठजोड़ होता है, तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत की टेलीकॉम सेवाओं पर नियंत्रण उस कंपनी का होगा जो सैटेलाइट फीड को नियंत्रित करेगी—इस मामले में मस्क की स्टारलिंक।
स्पेक्ट्रम क्या है?
अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, जो 2जी लाइसेंस विवाद के दौरान भी चर्चा में था। स्पेक्ट्रम क्या है और इसका टेलीकॉम या टीवी सेवाओं से क्या संबंध है?
जो लोग स्कूल की भौतिकी में स्पेक्ट्रम से परिचित हैं, वे जानते हैं कि विद्युत-चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगें, दृश्य प्रकाश, और उच्च-आवृत्ति वाली एक्स-रे और गामा किरणें शामिल होती हैं। 2जी से 5जी तक के लिए हम 900 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 26 गीगाहर्ट्ज़ तक के रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं।
पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के विवादास्पद 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के बाद, अब सभी स्पेक्ट्रम बैंड केवल नीलामी के माध्यम से ही दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2जी निर्णय में यह स्पष्ट किया कि स्पेक्ट्रम एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है और इसे केवल पारदर्शी और खुली नीलामी के माध्यम से ही आवंटित किया जा सकता है।
यहाँ तक कि पिछले साल मई में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के प्रशासनिक तरीकों से स्पेक्ट्रम आवंटन के प्रयास को खारिज कर दिया।
सरल शब्दों में, यदि स्पेक्ट्रम का उपयोग व्यावसायिक सेवाओं के लिए किया जाता है, तो इसे नीलामी के माध्यम से ही दिया जाना चाहिए।
एयरटेल और जियो का रुख़
दिलचस्प बात यह है कि पहले जियो और एयरटेल दोनों ने स्पेसएक्स के स्टारलिंक के सैटेलाइट आधारित संचार सेवाओं में प्रवेश का विरोध किया था।
- जियो ने स्पेक्ट्रम की खुली नीलामी का समर्थन किया था।
- एयरटेल ने प्रशासनिक आवंटन की बात मानी थी, लेकिन केवल 5 साल के लिए, जबकि स्पेसएक्स ने 20 साल का समय माँगा था।
दोनों कंपनियों के पास पहले से ही सैटेलाइट-आधारित सेवाओं के लिए साझेदारी है—जियो के साथ लक्समबर्ग स्थित SES और एयरटेल के साथ यूटेलसैट वनवेब।
अस्पष्ट स्पेक्ट्रम शुल्क
यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क कितना होगा और इसे कैसे निर्धारित किया गया है। यदि स्पेसएक्स जैसी कंपनियाँ उच्च गति इंटरनेट सेवाएँ शुरू करती हैं, तो क्या एक ही सेवा के लिए अलग-अलग शुल्क लगाए जाएँगे?
2जी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनज़र, सरकार बिना प्रतिस्पर्धी बोली के स्पेक्ट्रम कैसे आवंटित कर सकती है? और यदि शुल्क तय किए गए हैं, तो उन्हें किस आधार पर निर्धारित किया गया है?
कुछ अन्य मुद्दे
सैटेलाइट संचार से जुड़े कुछ अन्य मुद्दे भी हैं। मौजूदा अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट या सैटकॉम सेवाएँ भू-स्थिर उपग्रहों (Geostationary Satellites) द्वारा प्रदान की जाती हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की गति के समान गति से घूमते हैं और एक बड़े क्षेत्र में लगातार सैटकॉम सेवाएँ प्रदान करते हैं।
यदि अंतरिक्ष में उपग्रह और ज़मीन के बीच सापेक्ष गति होती है, तो सेवाओं में रुकावट से बचने के लिए उपग्रहों की एक श्रृंखला स्थापित करनी पड़ती है, जिसमें उपग्रहों के बीच समुचित तालमेल (हैंडशेक) होना चाहिए। इस तरह के निम्न-पृथ्वी कक्षा (LEO) उपग्रह बड़े क्षेत्रों में लगातार दूरसंचार सेवाएँ, विशेष रूप से ब्रॉडबैंड सेवाएँ, प्रदान करते हैं।
स्पेसएक्स के स्टारलिंक ने कक्षा में 7,000 से अधिक उपग्रह (satellites) स्थापित कर लिए हैं और आगे और भी भेजने की योजना है।
orbital space पर नियंत्रण का सवाल
अंतरिक्ष में किसे कितना कक्षीय क्षेत्र (orbital space) मिलेगा और कोई देश या इकाई कितना अधिकार कर सकती है, इस पर कोई नियामक या अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है। इस तरह के “जिसकी लाठी उसकी भैंस” दृष्टिकोण के दीर्घकालिक परिणाम चिंताजनक हो सकते हैं।
हालाँकि अंतरिक्ष में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वायुतरंगों (Airwaves) पर प्रतिबंध ज़रूर है। इसका मतलब यह है कि अंतरिक्ष से डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए जो वायुतरंगें इस्तेमाल होती हैं, वे संबंधित देश की संप्रभुता के अधीन होती हैं।
स्पेक्ट्रम लाइसेंस शुल्क का सवाल
यह सवाल महत्वपूर्ण है कि अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के लिए कंपनियाँ कितनी लाइसेंस फ़ीस चुकाएँगी। अब तक इस स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं हुई है।
पहले जियो ने स्पेक्ट्रम की नीलामी का समर्थन किया था, लेकिन अब देखना होगा कि वे वास्तव में क्या रुख अपनाते हैं। क्या वे भी एयरटेल की तरह प्रशासनिक आवंटन की वकालत करेंगे?
जियो और एयरटेल का रुख़ बदलने के कारण
अचानक जियो और एयरटेल का रुख क्यों बदल गया—पहले स्टारलिंक का विरोध और अब उससे गठजोड़? क्या इस “रिश्ते” में सरकार की कोई भूमिका है?
अमेरिका के दबाव और ट्रम्प की नीतियां
ये सवाल यहीं खत्म नहीं होते। हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका ने अन्य देशों के संसाधनों पर कब्जा करने, उच्च आयात शुल्क लगाने और महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को हड़पने की नीति अपनाई है। यह न केवल व्यापार युद्ध है, बल्कि एक तरह का नव-औपनिवेशिक संबंध भी है, जो औपनिवेशिक काल की वापसी का संकेत देता है।
इस दबाव के कारण ही पनामा को हांगकांग स्थित कंपनी से पनामा नहर के शेयर ब्लैक रॉक (एक अमेरिकी कंपनी) को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंपने की माँग की—नए राज्य के रूप में नहीं, बल्कि औपनिवेशिक संपत्ति के रूप में।
अमेरिका ने यूक्रेन से भी मांग की है कि वह अपने खनिज संसाधन अमेरिका को सौंप दे ताकि रूस के खिलाफ युद्ध में मिली अमेरिकी सैन्य और वित्तीय सहायता की भरपाई हो सके।
क्या भारत ट्रम्प को खुश करने के लिए कर रहा है समझौता?
क्या भारत द्वारा मस्क की स्टारलिंक को टेलीकॉम क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देना ट्रम्प को संतुष्ट करने का एक प्रयास है?
क्या इस नीति से अमेरिका के और अधिक माँगें नहीं बढ़ जाएँगी?
क्या यह नीति वास्तव में काम करेगी?
कमजोर होती अमेरिकी आर्थिक ताकत और वैश्विक प्रभाव
यह वह अमेरिका नहीं है जिसे फ्रांसिस फुकुयामा ने 1990 के दशक में नव-रोम और एकमात्र वैश्विक महाशक्ति के रूप में देखा था। यह वह अमेरिका है जो अपनी कमजोर होती अर्थव्यवस्था को कर-संग्रह या धमकी देकर सुधारने का प्रयास कर रहा है।
हमें यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि कमजोर होता वर्चस्वशील देश अधिक तर्कसंगत हो जाएगा—वास्तव में इसके उलट होता है। सत्ता का भ्रम उनकी आर्थिक गिरावट से कहीं अधिक धीमी गति से समाप्त होता है। यही वह खतरा है जो ट्रम्प पूरी दुनिया के लिए उत्पन्न करते हैं। इतिहास से हमने यही सीखा है।
Source: News Click